anubhav
मैं आंखों में
दर्द भर कर बैठी थी
अपनों के इंतजार में
वक़्त कहाँ
पहले अपने ढूंढ ले
फिर बैठियों इस बाजार में
यदि समय पर निभा लिया होता फ़र्ज़
वो तो सबको देही रहा था निरंतर
बस महेत्वकांक्षाओं में उलझ कर
आदमी ऐसा बना खुदगर्ज
कि अब तो दवा भी नाराज़ हो
कहीं घुल गई
रास्ता हमारा भूल गई
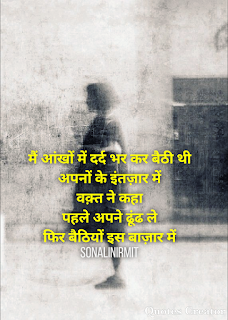




Comments
Post a Comment